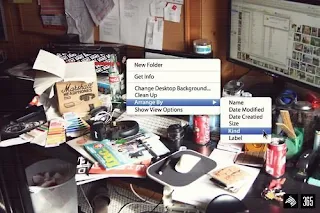अज़ब सी कैद है..
अंदर हूं तो भी डर लगता है
और बाहर जाने के ख्याल से भी
कि भला होता नहीं
और सकुचा हूं
किसी बुरे के मलाल से भी
अज़ब सी कैद है..
चुकानी हैं अभी
पालने—झूलने--
कच्ची उम्र की यादों की
किश्तें
कि.. और संजो लिये
नर्म रूई.. फाहे से रिश्ते
बुलाए हैं निर्दोष फरिश्ते
अज़ब सी कैद है..
एक—एक सलाख
बड़े जतन से बनाई है
लोहे,सोने—चांदी की जंजीरे सजाई हैं
अज़ब सी कैद है..
कि आजादी में
किसी तरह की कमी नहीं है
फिर भी हर सांस
अपनी मर्जी नहीं है
अज़ब सी कैद है..
कि चाहें ही नहीं है...
...ना आहें ही सहीं है
रंग भटके हुए हैं
बस वही कुछ काला है
कुछ सफेद है
अज़ब सी कैद है..
कि जिन्दगी की सजा
एक जुर्म है
कैद के बाहर
और भी जोखिम है..
जिस्म की मुसीबतें हैं
बेपर्दा ख्वाहिशों की
नापाक हकीकते हैं..
अज़ब सी कैद है..
हर याद और
हर रिश्ता एक दौलत है
इन पहाड़ों सी दौलत का बोझ
बस यही है
जो 'मैं' हूं
इनके सिवा
और कुछ भी नहीं हूं
किसी आजादी में
और
हर पल चाबुक हैं
संसार निभा!
संसार निभा!
अज़ब सी कैद है..
हर याद और
हर रिश्ता एक दौलत है
इन पहाड़ों सी दौलत का बोझ
बस यही है
जो 'मैं' हूं
इनके सिवा
और कुछ भी नहीं हूं
किसी आजादी में
और
हर पल चाबुक हैं
संसार निभा!
संसार निभा!